वो पलाश के, कॉमिक्स के, तिलस्म के....गर्मियों के दिन ।
पता नहीं क्यों मुझे गर्मियों का ये मौसम बहुत पुराने दिनों की याद दिला देता है । पिछले कई दिनों से मन बचपन की उस दुनिया में घूम रहा है जहां गर्मियां बड़ी तिलस्मी हुआ करती थीं । अपना बचपन यूं तो कोई बहुत क्रांतिकारी नहीं रहा, जिसमें आवारागर्दी की बहुत ज्यादा गुंजाईश हो.....लेकिन जैसा बीता है उसकी स्मृतियों की ऐसी सरगम आजकल छिड़ रही है कि क्या कहें ।
याद आते हैं बचपन वो दिन जो भोपाल में बीते । जब छुट्टियों की विकल प्रतीक्षा की जाती थी । योजनाएं बनाई जाती थीं और जब अचानक किसी धमाके की तरह छुट्टियां सामने आ जाती थीं तो सूझता नहीं था कि क्या किया जाए । सारी योजनाएं धरी रह जाती थीं । मई जून की वो ऊबी हुई, सुस्त, घुटी घुटी सी दोपहर बहुत याद आती हैं, जब घर में मां को सोते देखकर हम अकसर 'गली डॉक्टर आबिद' वाले उस घर से चुपचाप सटक लिया करते थे । फिर या तो छत पर जाकर कोनों में कीट-पतंगों की प्रतीक्षा करती गिजगिजाहट से भरी छिपकलियों पर नज़र डाली जाती थी, मुहल्ले की करामाती नालियों में नावें छोड़ी जातीं । या फिर छत की ओर जाती सीढियों पर पसरकर कॉमिक्स पढ़ी जाती थीं । आसपास के छर्रे-मित्रों से कॉमिक्स बदल ली जाती थीं । इस तरह दिन में कॉमिक्सों की इतनी खुराक हो जाती कि हज़म नहीं होती । फिर जब रात को नींद आती....जो ज़रा देर से ही आती थी....तो कभी मैन्ड्रैक की दुनिया में घूम रहे होते थे तो कभी चंद्रकांता-संतति के इलाक़ों में । लगता था कि हम भी ऐयारी सीख लेंगे और अभी चमत्कार करने लगेंगे ।
गर्मियों की दोपहर की वो मासूम आवारागर्दी बहुत याद आती है, जब मुहल्ले के बच्चे चोरी से फिल्म देखने जाते और हम सोचते कि काश हमें भी कभी चोरी से फिल्म जाने मिले तो कितना मज़ा आये । वो कार्टून फिल्मों और चैनलों के दिन नहीं थे । इसलिए टी.वी. का जीवन में कोई रोल नहीं था । मौज मस्ती के नाम पर बस इतना किया जा सकता था कि भरी दोपहर नींद के खुमार में डूबे किसी अलसाए घर की कॉलबेल टन्न से बजा दी जाये और चुपके से भाग जाया जाए । या किसी अंकल का स्कूटर न्यूट्रल पर करके स्टार्ट कर दिया जाये और भाग खड़ा हुआ जाए । बेचारा स्कूटर घुरघुराता रहे घंटों तक । पता नहीं क्यूं कुछ स्कूटर बिना चाभी के चालू हो जाते थे तब ।
तब मुहल्ले के कुछ घरों में भूत रहा करता था । एक घर तो अभी भी याद है जहां किसी महिला ने खुद को आग लगा ली थी, उस घर को भुतहा घर माना जाता था । पर दिक्कत ये थी कि वहां रहने वाले दोनों बच्चों को उनके पिताजी ने मां की कमी पूरी करने के लिए हिंद पॉकेट बुक्स की किताबों के बड़े बड़े सेट ला दिये थे । बचपन से ही मिज़ाज ऐसा था कि जो छपा हुआ पुरज़ा दिखे उसे ही पढ़ लिया करते थे । यानी समोसे अख़बार के जिस टुकड़े में लपेटकर लाये जाते अपन तेल से तर उस अख़बार को भी पढ़ लेते थे । पता नहीं पुराने अख़बार पढ़ने में क्या आनंद आता था । तो धर्मसंकट था । चुड़ैल वाले घर में जायें कैसे । कहीं कुछ हो गया तो । लेकिन आलमारी में जमी प्रेमचंद की किताबों का पूरा सेट आंखों के आगे तैर जाता था । आखिर प्रेमचंद चुड़ैल से जीत गये । छत पर जाकर दोनों घरों के बीच की दीवार को पार करके हम चुड़ैल वाले उस घर में जाते रहे और दोपहरों को प्रेमचंद की किताबों के पूरे सेट को एक एक करके पढ़ते रहे । सोचिए कि प्रेमचंद को उस भुतहे घर में पढ़ना ऐसा होता था जैसे किसी हॉरर फिल्म को देखना हुआ करता है । पता नहीं कब कहां से और किस तरह की प्रेतात्मा आ जाये, भूतनी, डाकिनी, चुड़ैल । इस तरह चंपक, चंदामामा और मधु-मुस्कान में हमने हॉरर मिलाकर पढ़ा ।
उन तिलस्मी दिनों की एक चीज़ और याद आती है । अकसर शाम को पिता गन्ने का रस पिलाने ले जाया करते थे । क्या माहौल खिंचा रहता था तब गन्ने के रस की दुकानों में । खस की पट्टी की बाड़ बनाकर लकड़ी की कुर्सियां और मेज़ें सजाई जाती थीं । शानदार लाल मेज़पोश । मद्धम संगीत और मेज़ पर रखी नमकदानी । बाहर बोर्ड लगा होता था फलानी मधुशाला । बड़े दिलचस्प नाम होते थे । और गन्ने के उस रस में बार बार नमक छिड़ककर पीने का आनंद दिव्य होता था । उन दिनों में थम्स-अप हमें कड़वा लगता और उस आदमी की बेची कुल्फी बहुत मीठी.....जिसका एक हाथ नहीं था....लेकिन ठेले के नीचे उसने घंटी लगा रखी थी जिसे बजाकर वो अपनी कुल्फी की बांग दिया करता था । वो दूधिया कुल्फी...गन्ने का वो रस....वो चीज़ें आज मैकडोनाल्ड और पेप्सी की आंधी में जाने कहां बिला गयीं ।
उन दिनों पिता शाम को अकसर बग़ीचों में ले जाते । अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी जाती । घंटों जूते के तस्में बांधे जाते । जो बार बार खुल जाते । फिर बांधे जाते । और पार्क में डूरेन्टा की झाडि़यों से बनी दीवारों और आकृतियों को देखकर अजीब-सा लगता । शहर भर के बच्चे पार्क में जमा होते । चकरियां, फिरकियां खरीदी जातीं । बुढिया के बाल खाए जाते । 'जॉय आईसक्रीम' और 'क्वालिटी आईसक्रीम' खाई जाती । पार्क के उस ओर हम देखते कि लिली टॉकीज़ में 'क़ातिलों के क़ातिल' लगी है । या गूंज बहादुर सिनेमा में 'खूबसूरत' लगी है । तिलस्मी फिल्मों होती थीं ये हमारे लिए । पार्क के दूसरी तरफ छोटा तालाब का पानी छप छप कर रहा होता था और वहीं नज़र आता बोट क्लब का ऑब्ज़रवेशन टावर । जिस पर चढ़कर हम लोगों को बोटिंग करते देखा करते थे । कभी नाव की सैर करने का मौक़ा जो मिलता तो डर के मारे हालत पतली हो जाती । लेकिन सारा शहर भोपाल के छोटे और बड़े तालाबों के आसपास बने पार्कों में आया करता था ।
शायद पलाश, कॉमिक्स और तिलस्मी गर्मियों के वो दिन आज भी मन की दुनिया में कहीं ठहरे हैं । तभी तो मुंबई की बजबजाई सी गर्मी में मैं उन सुहाने दिनों में घूम रहा हूं ।


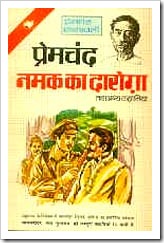
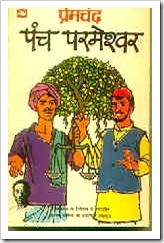


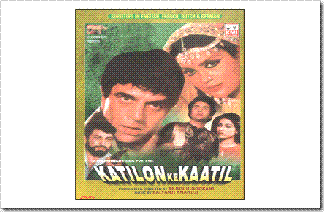





युनूस भाई ज़िन्दगी का वह दौर लौटे नहीं लौटता . आपकी ये पोस्ट हम सबके किशोर या युवा वय का फ़्लैशबैक है. अभी पिछले हफ़्ते मैंने अपनी जीजी (बुआ की बेटी)को एक चिट्ठी लिखी थी जिसके मज़मून मे से कुछ याद आ रहा है ग़ौर फ़रमाएँ:
जीजी फ़िर गर्मियों के दिन आ गए हैं और याद आ रहा है सैलाना (ज़िला रतलाम में मेरा मादरे वतन)के वे दिन बापूजी(मेरे दादा को दिया जाने वाला संबोधन) का तबला,पीछे बग़ीचे में अनार , सुरजना और अमरूद के बीच बिछीं वे खाट (सुतलियों से बुने पलंग)उस पर बाई (दादी) के हाथ की बनी वे महीन रज़ाइया,देसी आम का रस और चूल्हे बन बनी सिवैंया, कच्चे मकान मे पंखे की अनुपस्थिति और गर्मी को काटते वे ख़स के पर्दे...जीजी आज जीवन में सब है मोबाइल,एयरकंडीशनर,इंटरनेट कार....पर बापूजी-बाई के साथ बीतीं वो गर्मियाँ कहाँ ?(सनद रहे गर्मियाँ यहाँ द्वी-अर्थी है:मौसम की गर्मी और बुज़ुर्गों की मुहब्बत की गर्मी)गर्मियाँ अब भी हैं लेकिन खुलूस और गर्मजोशी के वे सिलसिले कहाँ...युनूस भाई थोड़ा याद रहा...पूरा जानना.
वाह;मजा आ गया । बिलकुल अपने खु़द के बचपन का शब्द-चित्र !
हाँ, एक बात में हम जरूर आपसे ज़्यादा खुशनसीब हैं। वो ये कि आज हर कमरे में ए०सी० लगे होने के बावज़ूद अपनी गर्मियों से बचपन की वो महक अभी गयी नहीं है । इस समय भी जब ये लाइनें टाइप कर रहा हूँ सामने खिड़की से दिखते;पीले और लाल रंगों के फूलों से लदे; अमलतास और गुलमोहर अपने पूरे शबाब पर हैं । भागते समय को मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश में हमने भी बचपन की नंदन,चन्दामामा,इन्द्रजाल कॉमिक्स,चंपक आदि के तमाम अंक ज़िल्दबन्दी करके तभी सहेज लिये थे, जिनकी सिलसिलेवार पूरी एक लाइब्रेरी आज भी है अपने पास । अब तो मेरे बच्चे भी उन्हें पढ़-पढ़कर बहुत बडे़ हो चुके हैं । फ़िलहाल तो इन्हें आगे कभी आने वाले पोते-पोतियों के लिये सँभाल रखा है ।
- वही
बचपन की याद आ गयी।
हाय पता नही आपने खेले थे या नही पर हमे तो कंचे भी याद आए ओर गुल्ली डंडा भी ओर लुटी हुई पतंगे भी.......
युनुस जी, आपने तो बचपन की बात याद दिला दी.. हमारी और आपकी पीढी में कम से कम 10-15 साल का अंतर होगा, मगर शायद सभी का बचपन एक जैसा ही होता है.. आपको पता नहीं होगा की मैं आज भी कामिक्स की दुनिया में खुद को गुमा हुआ पाता हूं.. कुछ कैरेक्टर बदल गये हैं मगर कामिक्स अभी भी उतना ही जादुई है.. और पढने के मामले में मेरे दोस्तों का कहना होता था की ये लड़का तो कोर्स की किताबों को छोड़कर सभी कुछ पढ जाता है, यहां तक की नोटिस बोर्ड भी.. :)
अरे युनुस भाई और बाल्टी भर-भर कर आम नही खाते थे क्या।
भाई हम भाई-बहनों मे तो होड़ लगती थी की कौन ज्यादा आम खा सकता है।
हम लोग तो मम्मी की साडियों का भी खूब कचरा करते थे।
बचपन पचपन से पैंसठ के दशक में भी ऐसा ही था। सबको नोस्टेल्जिक कर गए।
सही में नोस्ताल्जिक कर गए आप, प्रेमचंद और शरद्चंद को हमने भी बचपन में पढ़ा एक नहीं कई बार... वो सेट आज भी पड़ा है... धुल खा रहा है घर के आलमारी में...
ऐसा लगा कि खुद के बचपन के आंगन में खेल रहे हैं. वाह! यादों की गलियों में घुमना भी कितना सुखद होता है
आखिर प्रेमचंद चुड़ैल से जीत गये । :)
बहुत बढ़िया रहा पढ़ना.
सब की टिप्पणियाँ और आपका लेख पढ़ कर हमें भी अपना बचपन याद आ रहा है।
हम भी दोपहर की चिलचिलाती धूप की परवाह किये बिना; दिन को माँ की आँख लगते ही खेलने भाग जाया करते थे।
कॉमिक्स किराये पर चलाना तो मेरा सबसे पहला व्यापार था जिसमें मैने साथ रुपये कमाये थे... लागत मत पूछियेगा कितनी थी।
:)
मजा आ गया यूनुस भाई।
शानदार पोस्ट ! आपकी वज़ह से हम सब ने अपने बचपन की उन अलसायी दुपहरों को फिर से जी लिया।
यूनुस जी, आपके बचपन में कहीं भी हमें रेडियो नज़र नहीं आया।
अन्नपूर्णा जी ये बचपन की उन दोपहरों का जिक्र है जब रेडियो सुनने का संस्कार नहीं जागा था । तब तक हम गर्मियों की दोपहर में आवारागर्दी का लुत्फ लेते थे । बचपन में रेडियो पर क्या सुना लगता है :) इसके बारे में एक पॉडकास्ट करना होगा ।
aapke is post par meri dusari tippani..
maine shayad pichhali bar bataana bhool gaya tha..
aapne "Bahadur" vali comic ki tasveer lagaayi hai, shayad mere paas vo comic PDF format me hai.. agar aap kahen to main aapko bhej dun?? :)
Post a Comment